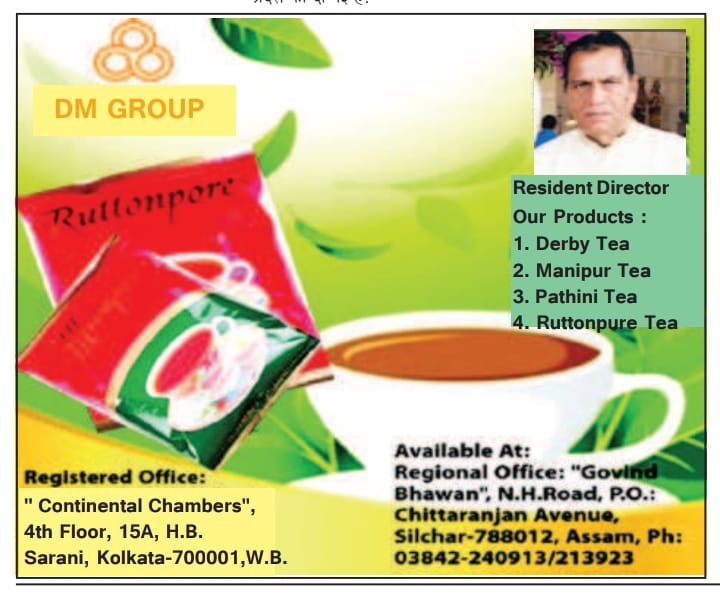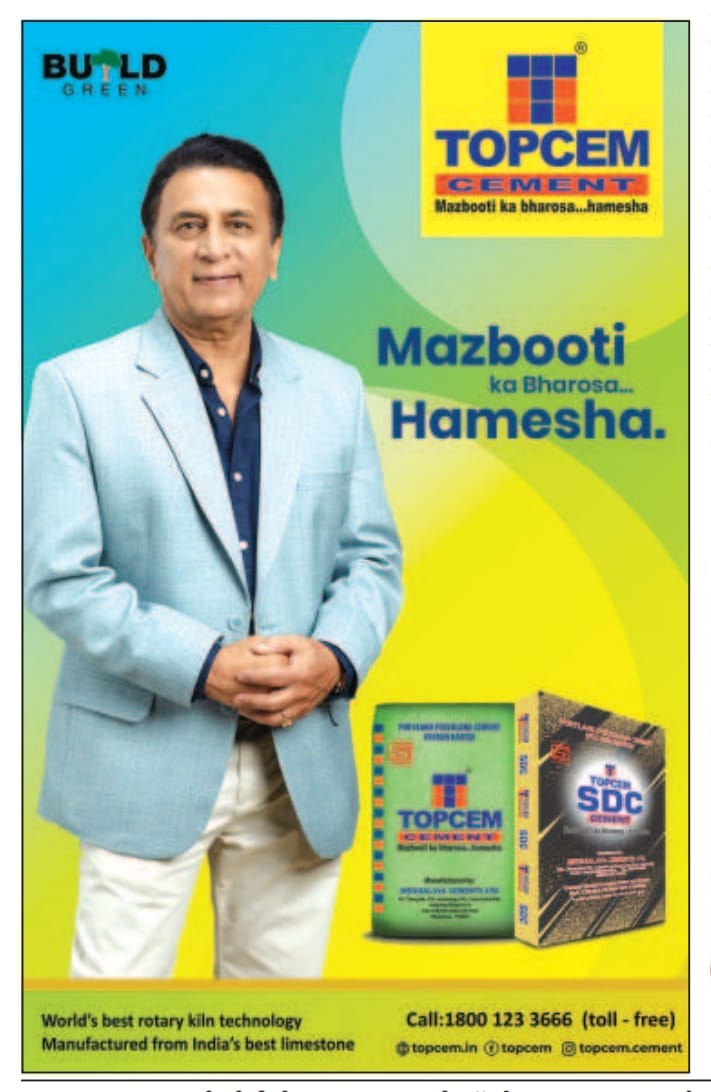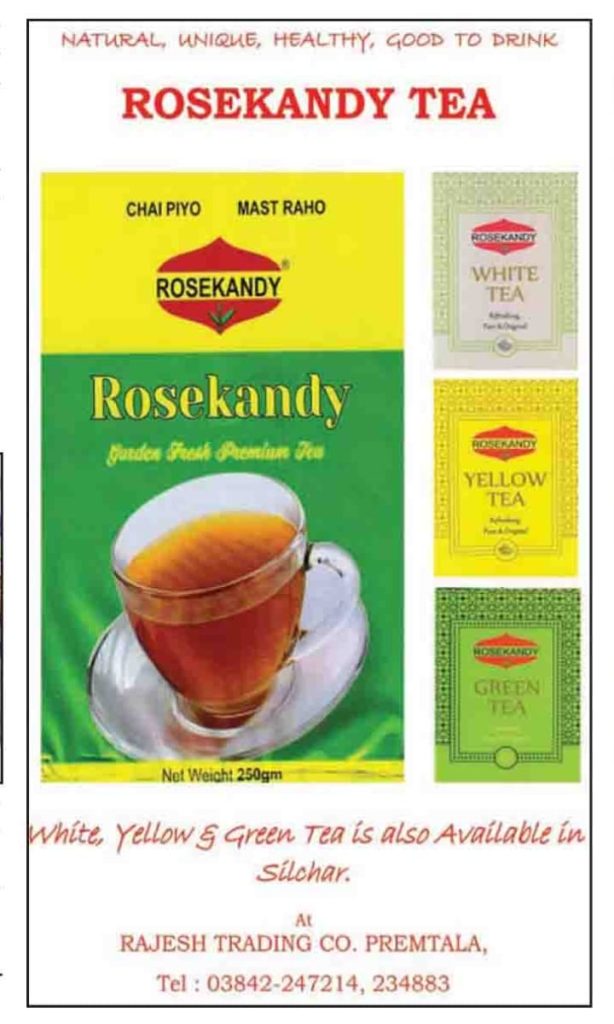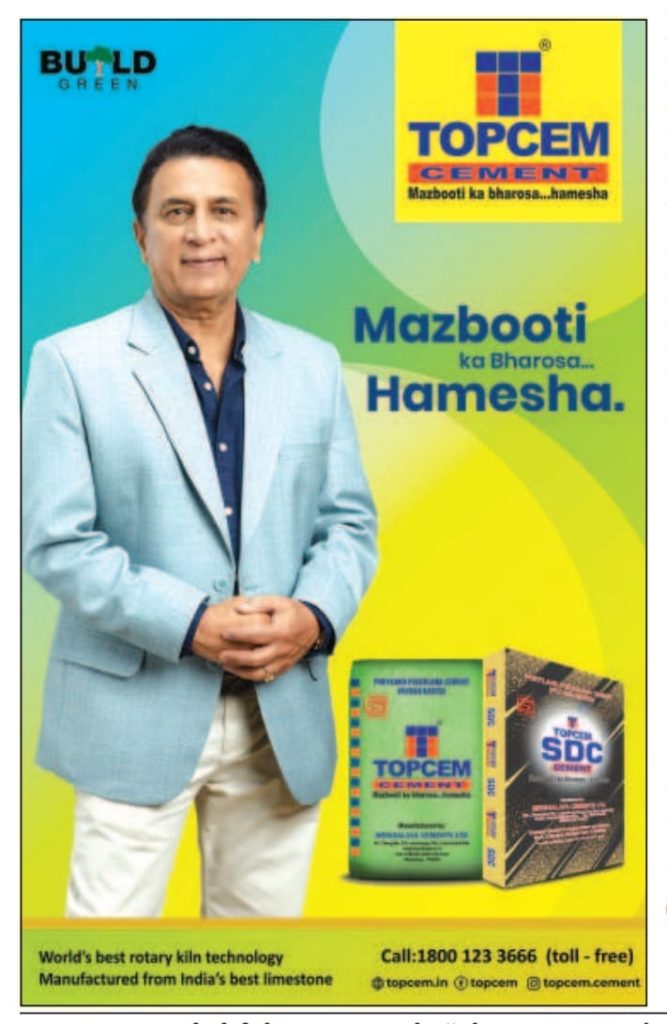284 Views
गड़रिए
अक्सर निर्जन में रहते हैं
प्रकृति के ख्यालों में गुम रहते हैं
वनस्पतियों, पेड़-पौधों से बतियाते
बतियाते ढ़ोर से
धरती की हर कोर से
पहाड़,पठार और मैदान
झीलों, नदियों, आंधी-तूफान, खग
भ्रमर, तितलियों और मधुमक्खियों से बतियाते
बतियाते जल, नभ और थल से
रम-बस जाते
दिन में सूरज और धरती से
डंगर -ढ़ोर के बीच
रात में चांद, तारों और आकाशगंगा से बातें करते
रेवड़ की गंध में
महसूस करते सुरभि
और महसूस करते बारिश में मिट्टी की सौंधी खुशबू
मेंड़ों और पगडंडियों पर बैठ मुस्काते
हाथों में लाठी लिए
सूखी मोटी और बासी रोटी और सिलबट्टे पर रगड़ी हुई
चटनी और
पानी की छागल लिए
उनके सिर पर अक्सर एक फटा पुराना गमछा बंधा होता है
उम्मीद की किरणें अपने साथ लिए
धरती जिनका बिछौना और आसमां ही छत है
शीत और ताप से बेपरवाह
ईश्वर का शुक्र मनाते
अपने आप में मदमस्त
वे आम आदमी की भांति पदार्थ में नहीं रहते
उनके झुलसे चेहरों में एक चमक होती है
संतोष के भाव होते हैं
वे शिकायत नहीं करते
वे एक दूसरे को कोसते नहीं हैं
शिकायत,गिले-शिकवे उनके पास नहीं फटकते
जमाना जहां
पदार्थवादी बना है
उसी जमाने में वे हर ऱोज
संतोष का सूरज उगाते हैं
वे गोधूलि में
सुबह और शाम की रंगीन फिजाओं में खो जाते हैं
वे धन -दौलत में नहीं
संतोष और सुख में जीते हैं।
सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।