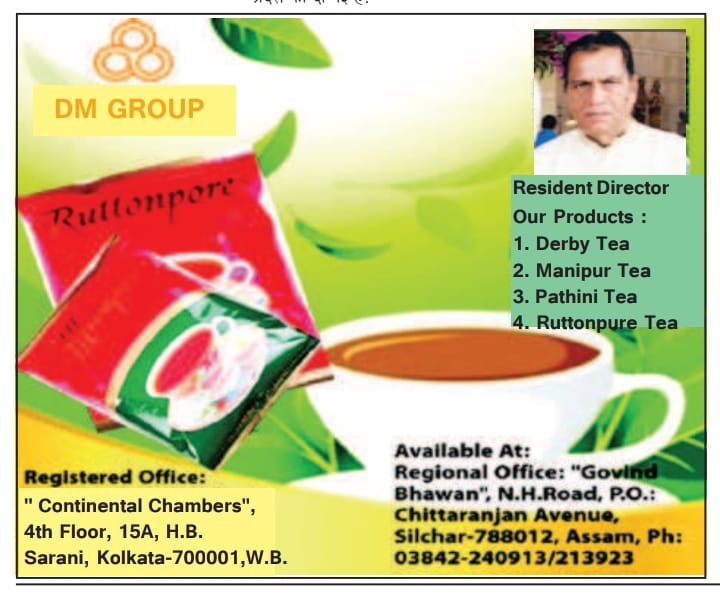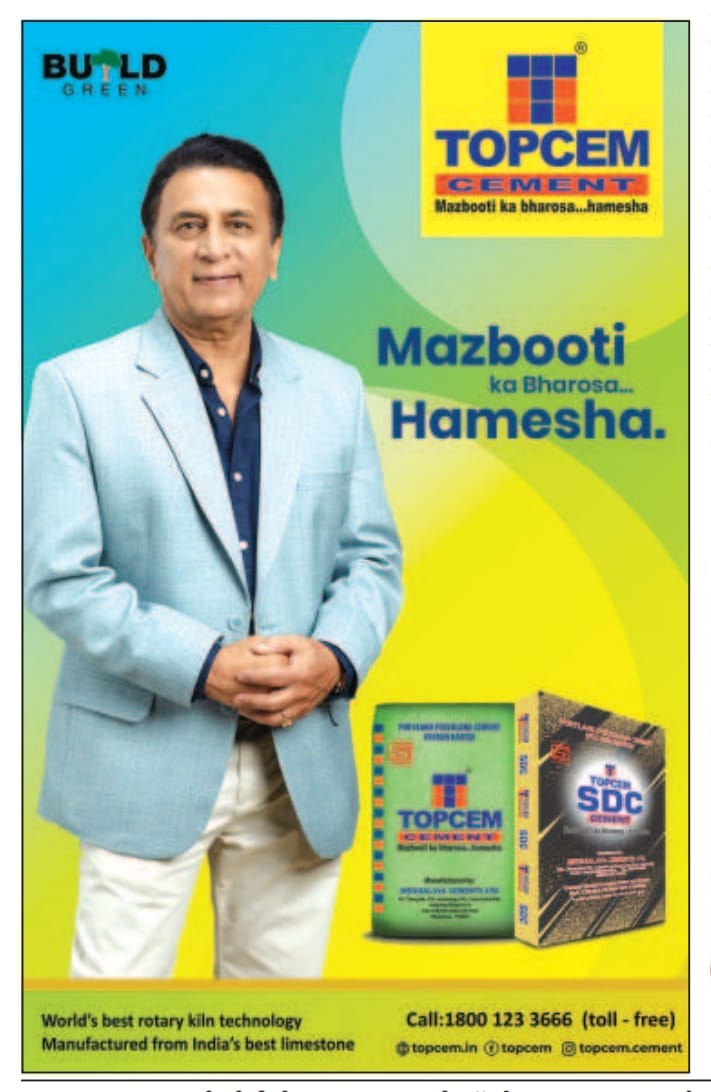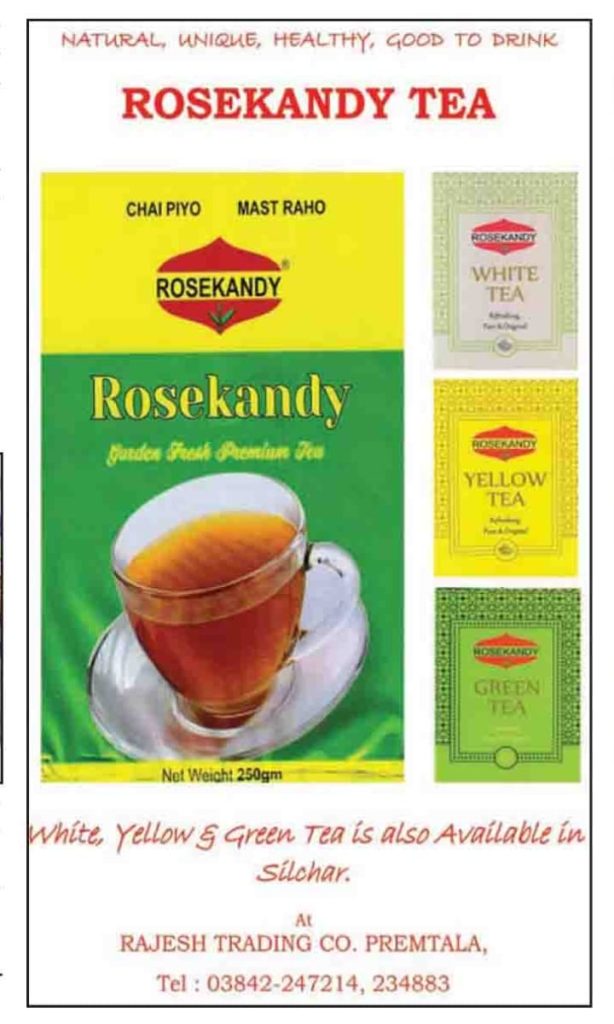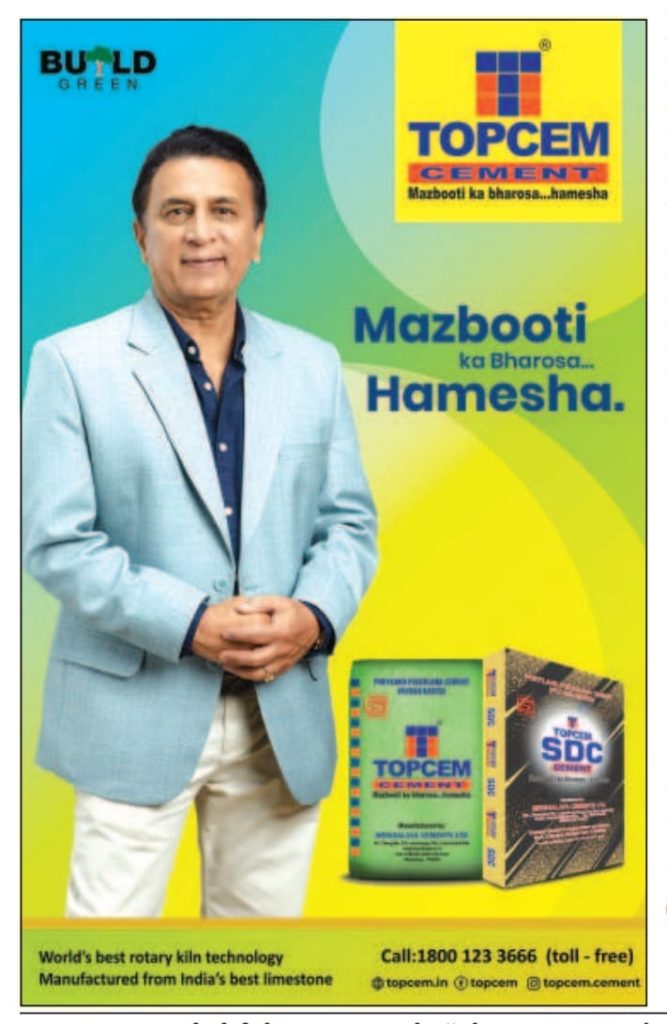प्निय मित्रों ! नित्यसत्यचित्त बुद्धमुक्त पदऽस्थित तथागत महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेशित-“धम्मपद्द” के भावानुवाद अंतर्गत स्वकृत बाल प्रबोधिनी में चित्त वग्गो के छठवें पद्द का पुष्पानुवाद उनके ही श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूँ–
“अनिवट्ठित चित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो ।
परिप्लवपसादस्स पञञा न परिपूरति ।।६।।”
अब पुनः कहते हैं कि–
“अनिवट्ठित चित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो”
अर्थात “बुद्धत्व” प्राप्ति की पहली शर्त है आजीवन पर्यन्त चित्त का आत्मस्थ रहना ! जिनके जीवन में संयम नहीं है ! और यदि है भी तो वह भी जबरदस्ती का थोपा हुवा संयम ! तो यह तो और भी ज्यादा भयावह हास्यास्पद और अधोगामी होगा ! मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पड़ी नहीं कर रहा किंतु एक छोटा सा उदारहण देता हूँ-“दूरंगमं एकचरं असरीरं गुहासयं।”
मैं बचपन से ही जिनके प्रति कुछ श्रृद्धा रखता था ऐसे ही एक किसी समय की महान वीभूति आज कई वर्षों से जेल की चहारदिवारियों में कैद हैं ! जिनके कम से कम एकाध करोण शिष्यादि थे उनके समर्थन में धीरे-धीरे सभी शांत होते जा रहे हैं।
मैं मानता हूँ कि ऐसा ही कुछ बहूत से महापुरूषों अथवा कथित-महापुरूषों के साथ भी हुवा होगा ! किंतु उस प्राचीन काल में भी उन्हें सजा देने वाली न्याय व्यवस्थाऐं उन्हें सजा देकर तत्काल ही अपने दायित्व का निर्वहन करती भी थी ! किंतु इन महापुरूष के साथ तो ऐसा नहीं ही हो पा रहा है ?
न्याय व्यवस्था तो क्या कृमशः उनका शिष्य समुदाय भी आत्मग्लानि से अपने आपको असहज सा कहीं न कहीं तो पा ही रहा है ! हाँ मित्रों ! चित्त की चंञ्चलता बड़े-बड़े महापुरूषों को भी एक पल मात्र में अधोगामी बनाने में सक्षम् है ! यदि मैं अपने आपको बल पूर्वक विषयों में जाने से रोकता हूँ-और अंतःकरण उन्ही विषयों की तरफ भागता है तो “ऐसा तो होगा ही !” और इस भटकाव का कारण क्या है—-
एक दिन ये कुछ कागज छिपाकर रख रही थीं ! मुझसे बोलीं कि आप इन कागजों को देखने की कोशिश मत करना ! ये आपके लिये या मेरे लिये भी देखने योग्य नहीं हैं ! बस उसी पल से मैं बेचैन हो गया ! क्या है इन कागजों मे ?
और जैसे ही ये कहीं बाहर गयीं,कि तत्काल मैं उन कागजों को ढूँढ-कर देखने बैठ गया ! अर्थात जबरदस्ती का अपने आप पर थोपा हुवा संयम भी कुछ ऐसा ही होता है ! संयम का पालन तो तभी हो सकता है जब उन विषय भोगों के प्रति चित्त “संशयग्रस्त”न हो।
मुझे अपने आपको समझाने की नहीं बल्कि यह समझ लेने की आवश्यकता है कि “विषय और विष” एक दूसरे के पर्याय हैं ! मुझे- “कर्तव्याऽकर्तव्यः” का बोध होना चाहिये ! अपने उन दुर्भाग्यपूर्ण पलों का स्मरण होना चाहिए जब मैं दुर्व्यसनों के अधीन था ! मुझे भलीभांति उन दिनों का आज भी स्मरण है जब मैं बीडी,सिगरेट,गाँजा,भाँग आदि का नियमित सेवन करता था ! अत्यधिक सेवन करता था ! भगवान के नाम पर करता था ! उनकी अपेक्षा वे दिन बहुत ही अच्छे थे जब बचपन में मैं अपने
पेट भरने के लिये मुम्बई चर्चगेट पर बूट पाॅलिस करता था ! और मुम्बा देवी सडक पर गटरों की सफाई करता था।
मित्रों ! अब यदि मैं अपने अनुष्ठेय धर्म के तात्पर्य को नहीं जानता ! तो उनका पालन करूँगा कैसे ? इसी सन्दर्भ मे-
“अनादानविसर्गाभ्यमीषन्नास्ति क्रिया मुनैः।
तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु।। वि.चू.२८३।।”
में आद्य श्री शंकराचार्य जी कहते हैं ! अब आप इतना ही विचार करें कि-बुद्ध पुरूषों के मन में अन्न का गृहण करना-और मल विसर्जन कर देना” का किंञ्चित मात्र भी भाव नहीं रहता ! उनका उन क्रियाओं के प्रति कोई लगाव होता ही नहीं ! अर्थात
भोजन करने से तात्पर्य निगल लेना मात्र नहीं है ! पहले तो मैं अन्न लाता हूँ,फिर पात्र ! तदोपरान्त उसे बनाने की योजना ! स्वाद की कल्पनादि सभी की सभी क्रियाऐं”अनादान के अंतर्गत ही आती हैं-और उनका अंतिम परिणाम अंततः मल-विसर्जन ही है।
मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितनी भूलें कर चुका ! जितने गलत कदम उठा चुका ! उठा चुका ! अब उन भूलों को सुधारने की कोशिश करना है ! उन कदमों के चिन्ह मिटाने हैं ! मैं कहना चाहता हूँ कि अपने किये पुण्य कर्मों को भुलाना इससे भी अधिक आवश्यक है ! पापकर्म के फलस्वरूप मिलते दुःखों की अपेक्षा पुण्यों से मिलने वाले सुख एवं उन सुखों की कल्पना और भी अधिक भयानक है ! तात्पर्य यह है कि बुद्ध पुरूष न-“अनादान” की चिंता करते हैं और न ही- “विसर्जन” की और यही स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन भी है।
मित्रों ! जिस प्रकार अधिकांशतः पशु-पक्षी, नभचर,जलचर और थल-चर जीव यथासम्भव संग्रह करना जानते ही नहीं ! वो प्रकृति की गोद में निश्चिंत हैं ! भय,आहार,निंद्रा और मैथुन मानव की तरह उनमें भी जन्मना है ! किन्तु उनमें हम तथाकथित मानवों की तरह-“साम,दाम,दण्ड और भेदकारी दुष्प्रवृत्तियाँ किंचित भी नहीं हैं ! किन्तु उनकी अपेक्षा हम जो- “परिप्लवपसादस्स पञञा न परिपूरति” अर्थात चंञ्चल मन होते हैं ! अस्थिर बुद्धि के होते हैं ! जिनमें संकल्प शक्ति का अभाव होता है ! उनमें तो बस-“अनादान और विसर्जन”की चिंताऐं और प्रवृत्तियाँ उन्हें विषयादि भोगों के चिंतन में बारम्बार प्रवृत्त करती रहती हैं, परिणामतः वे- “आत्मबोध”में न स्थिर रह पाते हैं और न ही आत्मविशयक ज्ञान को ही प्राप्त कर पाते हैं !यही इस पद का भाव है ! शेष अगले अंक में प्रस्तुत करता हूँ–“आनंद शास्त्री सिलचर, सचल दूरभाष यंत्र सम्पर्क सूत्रांक 6901375971”