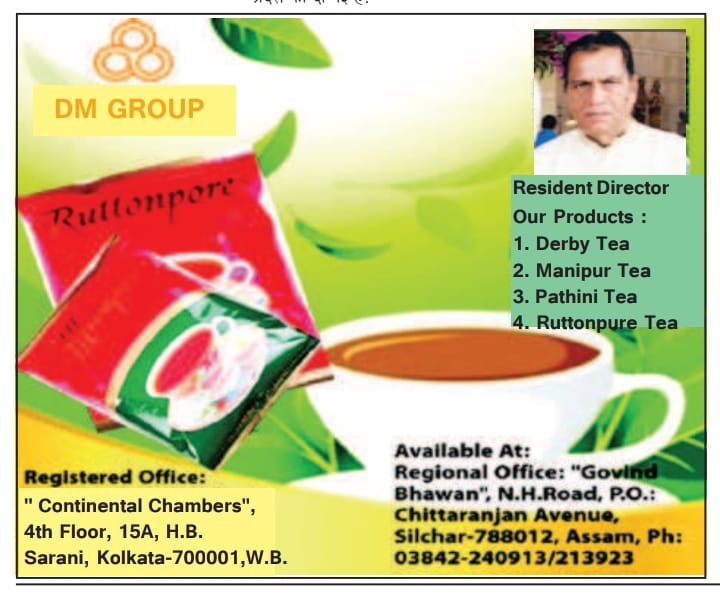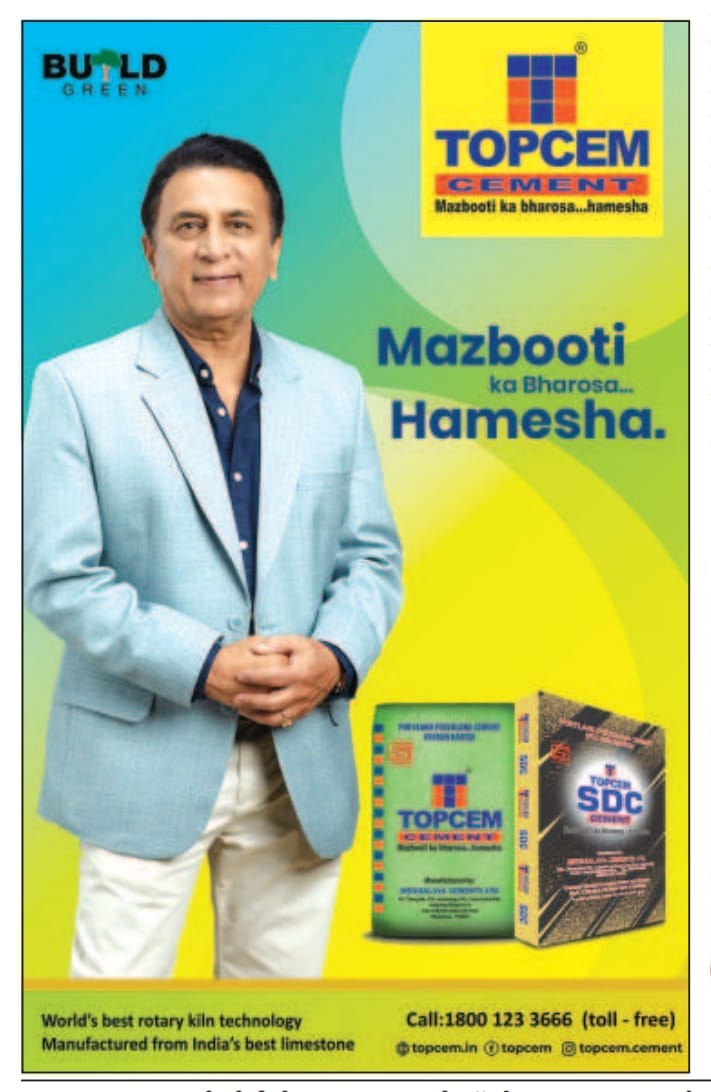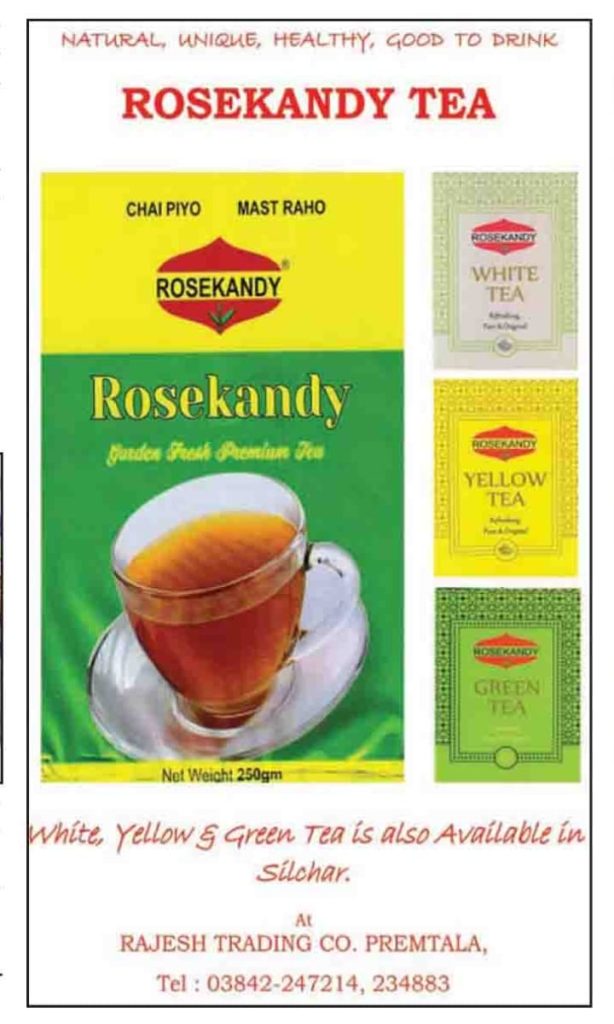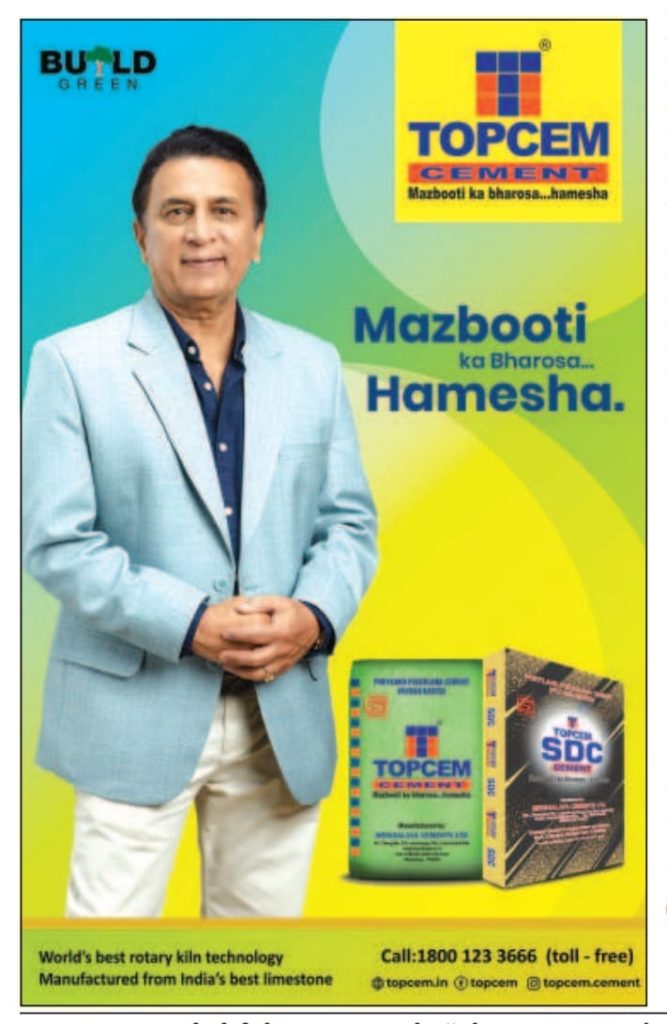137 Views
एक टीस नहीं, एक कसक है जो कलेजे में चुभती है,
जब कोई बेख़बर आकर कहता है:
“एक और कर लो, घर पूरा हो जाएगा!”
समाज का गणित है—
स्त्री का जीवन सफल हो जाता है,
जब उसके आँचल में दो या दो से अधिक फूल खिलते हैं।
पर कोई नहीं देखता
कि उस स्त्री के माथे पर कितनी अपेक्षाओं का पहाड़ टिका है,
कितने अधजले ताने उसे रोज़ पीने पड़ते हैं।
अकेले एक हो, दो हों, या तीन—
इन नन्हे जीवों को पालने की लड़ाई में
वह आटा पीसती मशीन सी चलती जाती है।
शरीर तो क्या, उसकी भीतर की रोशनी तक बुझने लगती है।
कंधे, कमर, हाथ, घुटने—
सब उम्र से पहले जवाब देने लगते हैं।
अपनी खिलती काया की सुंदरता, वह
इन एक, दो, तीन, चार हंसते चेहरों पर कुर्बान कर देती है।
रात-दिन खुद को तिल-तिल जलाती है,
और बदले में मिलते हैं यही शब्द:
“दिन भर करती क्या हो? तुम्हें कौन-सा काम है?”
“तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं बची।”
मगर बिन बुलाए राय देने वालों का बाज़ार गर्म है।
ये भूल जाते हैं कि सिर्फ़ औरत ही नहीं बच्चे का संसार,
जो पिता बना है, उसे भी तो अपना वचन निभाना है!
वे बच्चे, जो कभी फिसलते घुटनों पर चलते थे,
बड़े होकर दे जाते हैं
माँ को ही उम्र भर का घुटनों का दर्द।
पिता तो बस पैसे की दीवार खड़ी करने में मशगूल है,
कभी ग़लती से चौखट पर आ भी जाए,
तो माँ की ही मेहनत का हिसाब लेता है।
और फिर बुढ़ापे में—
सब एक-एक कर नई मंज़िल चुन लेते हैं,
पीछे रह जाती है वह थकी हुई आँखें वाली स्त्री,
और सीने में धँस जाती है उसकी टीस।
तब वह सोचती है:
काश! यह माथे की लकीर न बनी होती।
काश! वह भी एक खेलती बच्ची बन
हमेशा के लिए माँ के आँचल में सिमटी रहती।
कभी-कभी एक पल आता है, जब वह सोचती है—
‘चलो, दे ही देती हूँ इसको एक साथी और।’
लेकिन तुरंत ही सच की चोट लगती है:
“ये तो लड़की है!”
बड़ी होकर तो यह डोर कटते ही उड़ जाएगी।
फिर यह तरसेगी:
बहन संग घर-घर का खेल खेलने को,
भाई के माथे पर ‘दूज’ का टीका लगाने को,
पिता के साथ बेफ़िक्र बाज़ार जाने को,
माँ संग त्योहारों की मिठास बाँटने को।
यह कैसा अन्याय है इस समाज का!
जिसने हर बेटी को,
ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही पराया धन बना दिया।
डॉ मधुछन्दा चक्रवर्ती
बंगलुरू 36