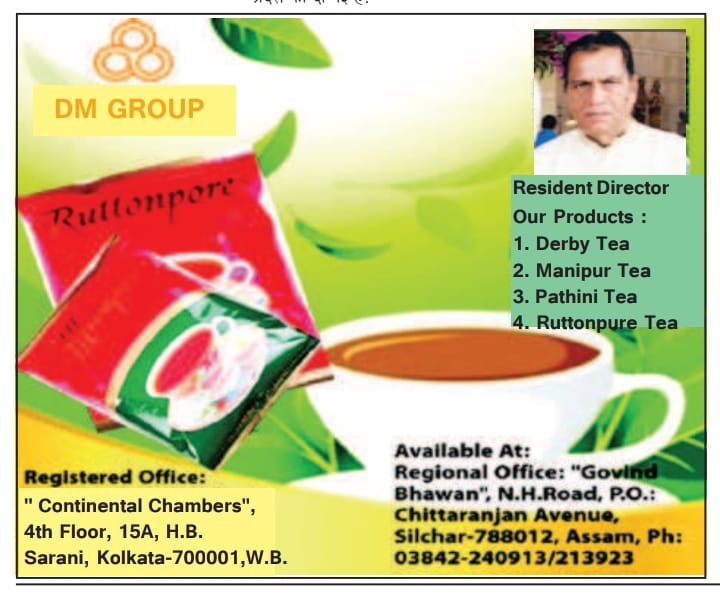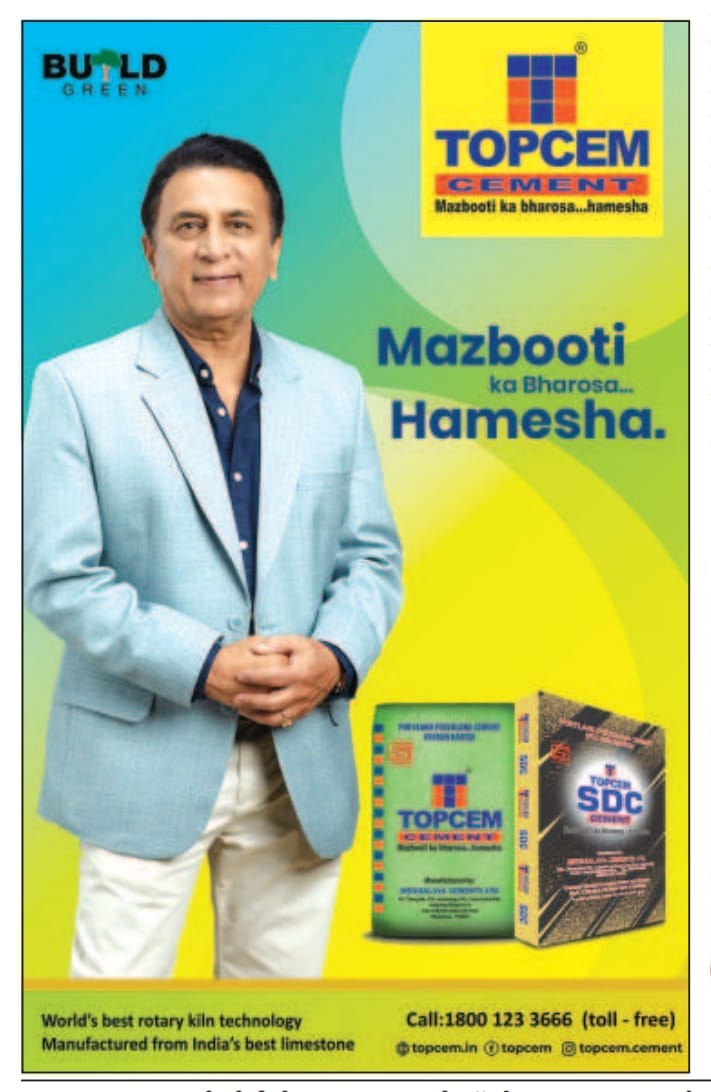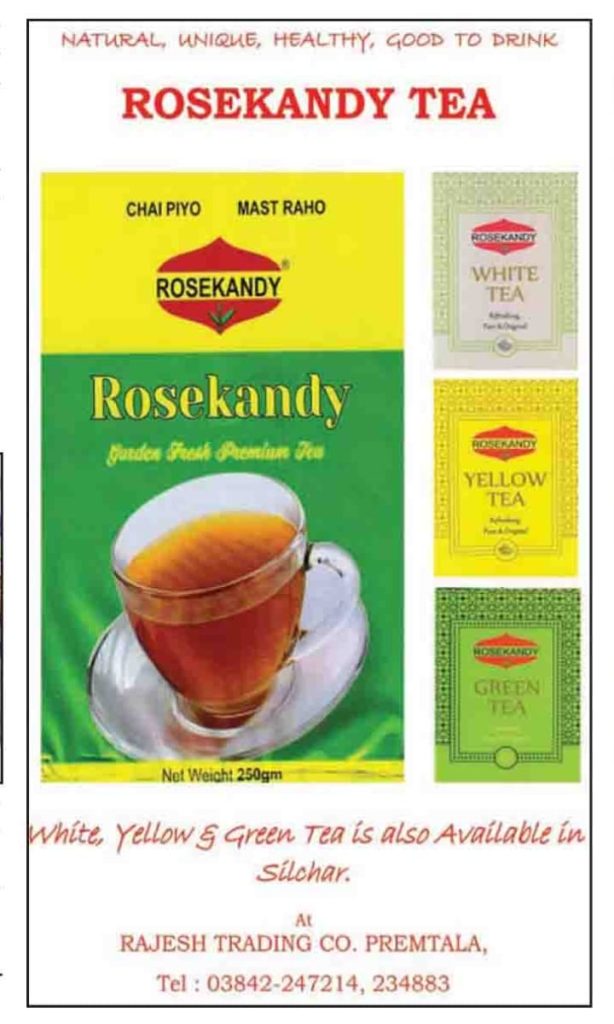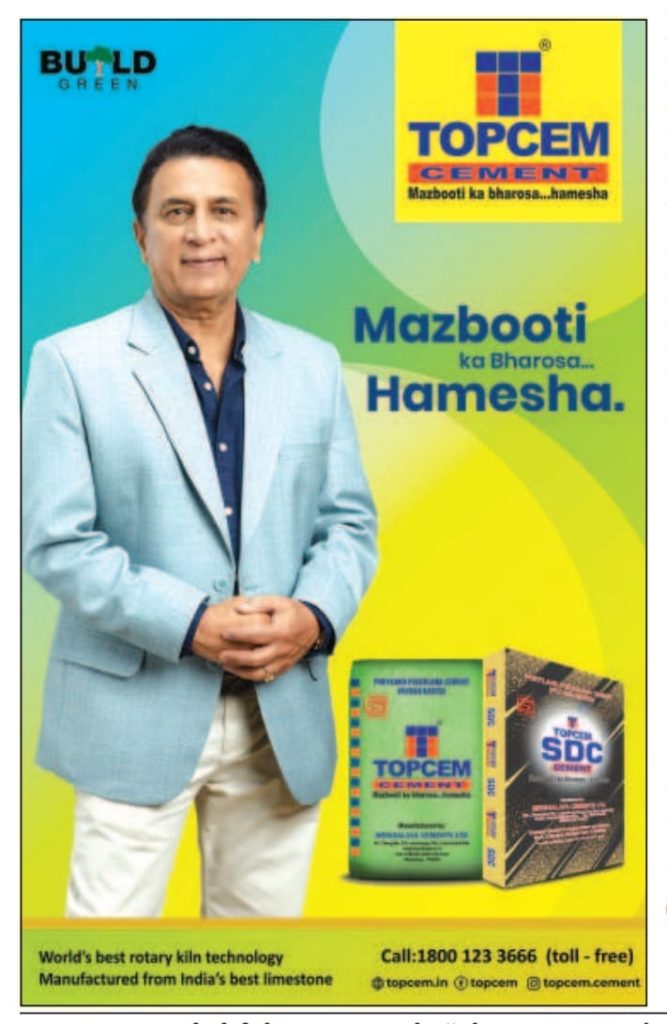रामचरितमानस में एक स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं – जेहि का जेहि पर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलहिं न कछु सन्देहू अर्थात् जिसको जिस चीज़ से सच्चा प्रेम होता है उसको वह चीज़ अवश्य मिल जाती है इसमें संदेह नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि सच्चे मन से चाही गई वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। प्रेम से हम किसी को पा सकते हैं, अपना बना सकते हैं। ईश्वर को भी। इस बात को हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि हम जो चीज़ भी पाना चाहते हैं उसे मन की गहराई से अथवा सच्चे मन से
चाहें। अगर हम सच्चे मन से किसी चीज़ को चाहेंगे तो वह अवश्य ही उपलब्ध हो जाएगी। प्रेम सच्चा हो तो मिलन में देर नहीं लगती। हमारी सच्ची चाहत ही वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को आकर्षित कर उन्हें सुलभ बनाती है। उत्तम स्वास्थ्य अथवा
प्रसन्नता भी इसका अपवाद नहीं। यदि हम अच्छे स्वास्थ्य व प्रसन्नता की कामना करेंगे तो परिस्थितियाँ अच्छे स्वास्थ्य व प्रसन्नता के अनुकूल होकर हमारी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हो जाएँगी। गोस्वामी तुलसीदास ने ये भी कहा है – जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी अर्थात् जैसी हमारी भावना होती है भगवान का स्वरूप भी वैसा ही होता है। हमारी भावना ही हमारे ईश्वर का निर्माण करती है। आज तक किसी ने ईश्वर को नहीं देखा लेकिन फिर भी अनेक लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा है या उसकी उपस्थिति को अनुभव किया है। यही तो भावना है। भक्ति भी वास्तव में हमारी भावनाओं के अनुरूप ही होती है। भाव ही भक्ति है इसमें संदेह नहीं लेकिन ये भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? फिर हम जिन भावों का पोषण कर रहे हैं वे ठीक भी हैं या नहीं? एक और प्रश्न उठता है कि भक्ति ही क्यों? भक्ति से क्या मिलेगा? जिसके परिणामों का ही पता नहीं चलना उस परीक्षा के लिए सर खपाने की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़नी शुरू होती है लोग धर्म-अध्यात्म की ओर झुकने लगते हैं। भक्ति उसी का ही एक रूप है। लोगों की कुछ ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है कि वे समझते हैं
इस संसार से मुक्ति के लिए भक्ति ज़रूरी है। वैसे इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मोक्ष जैसी कोई स्थिति होती है और भक्ति इसमें सहायक होती है। उम्र बढ़ने के अनुभव के साथ-साथ मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है कि ये भक्ति आदि सचमुच समाज की कंडीशनिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन कोई भी स्थिति एकदम निरर्थक नहीं होती। भक्ति भी नहीं। ये अलग बात है कि इसको बिलकुल भी न जानने-समझने वाले भी अपने निहित स्वार्थों के लिए इसका महिमामंडन करने के लिए पूरा ज़ोर लगा देते हैं क्योंकि आज ये एक बड़ा लाभदायक व्यवसाय हो गया है। इससे अर्थ लाभ भी होता है और लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है। हाँ तो बात हो रही थी कि भक्ति भी एकदम निरर्थक नहीं होती। भक्ति या भक्ति का आंतरिक भाव कह लीजिए हमारे लिए लाभदायक होता है क्योंकि ये एकाग्रता और अनुशासन उत्पन्न करता है। इससे हमारे जीवन में न केवल नैतिकता का विकास होता है अपितु इससे सामाजिक व्यवस्था भी सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलती है। यदि भक्ति भावना अथवा पूजा- पाठ से हमारे जीवन में धर्म का विकास नहीं होता तो ऐसी भक्ति भावना अथवा पूजा- पाठ निरर्थक है। पाखंड है। धर्म से तात्पर्य अनुशासन व सद्गुणों के विकास से है। धर्म अच्छी आदतों का समुच्चय है और कुछ नहीं। फिर भी यदि हम कहते हैं कि भाव ही भक्ति है तो बात कुछ अधूरी सी रह जाती है। भाव तो हर चीज़ के पीछे होता है। अच्छाई के पीछे भी भाव होता है तो बुराई के पीछे भी भाव ही होता है। भाव भक्ति है तो भाव ही कर्म है। भाव ही आस्तिकता है तो भाव ही नास्तिकता है। भावों में सकारात्मकता भी हो सकती है तो नकारात्मकता भी हो सकती है। भाव ही सर्जक हैं तो भाव ही विध्वंस के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। भक्ति को साधना भी कहा गया है। जीवन में यदि कोई महत्त्वपूर्ण साधना है तो वो है भावों के परिष्कार की साधना। भावों को सँवारना अथवा उन्हें सकारात्मकता प्रदान करना ही जीवन को सँवारना है। यदि भक्ति इसमें सहायक नहीं होती है तो ऐसी भक्ति मात्र छलावा है, पाखंड है। समाज को और स्वयं को धोखा देना
है।
एक प्रश्न और उठता है कि भावों की उत्पत्ति कैसे होती है? कहाँ से होती है? भावों की उत्पत्ति होती है विचारों से। विचारों से भाव और भावों से सभी परिस्थितियों व भौतिक वस्तुओं का निर्माण होता है। यदि परिस्थितियों, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं
तथा भावों को सही करना है तो विचारों को सही करना होगा और विचारों को सही करने के लिए विचारों के उद्गम तक जाना होगा। विचारों का उद्गम है मन। मन की साधना द्वारा ही हम भावों को सही आकार दे सकते हैं। अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। मन की
साधना भी मन द्वारा ही होती है। मन साधन भी है और साध्य भी। यदि मन द्वारा मन को वश में करके हम भावों को सुंदर व सार्थक बना सकते हैं तो अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आज हम धर्म अथवा भक्ति के मूल तत्त्व को भूल गए हैं।
हमारा ध्यान केवल कर्मकांड अथवा दिखावे पर होता है। हम बाह्याडंबरों को धर्म- अध्यात्म व भक्ति से जोड़ने लगे हैं। ऐसे धर्म-अध्यात्म अथवा भक्ति का कोई लाभ नहीं। अपनी बात पर ज़ोर देने के लिए हम कुतर्क करने लगते हैं। हम कहते हैं भक्ति शुद्ध मन अथवा अंतःकरण से होनी चाहिए। यही मेरा मानना है कि मन शुद्ध होना चाहिए। यदि मन में विकार भरे हों तो ऊपर से चीखने-चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। मन का विकाररहित अथवा निर्मल हो जाना सबसे बड़ी बात है। हमारी साधना मन को सुंदर
बनाने के लिए होनी चाहिए। मन सुंदर है तो किसी पाखंड की ज़रूरत नहीं। वास्तव में वे लोग ज़्यादा नाटक करते हैं जिनके मन विकारग्रस्त होते हैं। ऐसा वे सामान्य लोगों पर प्रभाव डालने के लिए करते हैं। यदि भक्ति किसी पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से की
जाए तो भक्ति ही नहीं रहती। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि जितने भी तथाकथित नाटक करने वाले भक्त हैं उनमें सामान्य लोगों से अधिक गड़बड़ियाँ मिलती हैं। प्रायः ऐसे लोग मान लेते हैं कि भक्ति का ठप्पा लग जाने से उन्हें विशेष व्यक्ति का दर्जा मिल गया है। लोगों से उनकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं। वे चाहते हैं कि उनकी धार्मिकता के कारण लोग उन्हें विशेष
महत्त्व दें। उनका विशेष सम्मान करें। लेकिन क्यों? क्या इसी लिए आपने भक्ति मार्ग का अवलंबन किया है? यदि आपका यही उद्देश्य है तो आपकी भक्ति निकृष्ट से भी निकृष्ट श्रेणी की है। लोगों पर प्रभाव डालने अथवा मोक्ष वगैरा की कामना के लिए स्वयंनिर्मित भगवान की चापलूसी करना छोड़कर यदि हम विकारों से मुक्त होने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाएँ तो अधिक श्रेयस्कर होगा। इससे ही सुंदर समाज के निर्माण में सहायता मिल सकती है।
सीताराम गुप्ता,
ए.डी. 106 सी., पीतमपुरा,
दिल्ली – 110034
मोबा0 नं0 9555622323
Email : srgupta54@yahoo.co.in